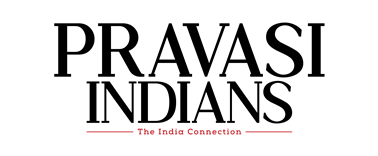तरह तरह की दुविधाओं से घिरे प्रवासी भारतीय चाह कर भी अपने देश की सेवा नहीं कर पाते। अपनी धमनियों में बहने वाली भारतीय संस्कृति और परंपरा से जुड़ कर तथा उन अनुभवों को साझा कर वे संभवतः बहुत हद तक इस ग्लानि से बच सकते हैं। प्रवासी भारतीयों का अपनी मिट्टी से अलग होने का वियोग और उनसे जुड़े कड़वे अनुभवों को उकेरता यह आलेख।
मणीन्द्र नाथ ठाकुर
लेखक जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के राजनीतिक विज्ञान के प्राध्यापक हैं और भारतीय ज्ञान-परंपरा और राजनैतिक-चिंतन के सामयिक पक्षधर रहे हैं। इनकी एक पुस्तक ज्ञान की राजनीति: समाज अध्ययन और भारतीय चिंतन अभी अभी प्रकाशित हुई है।
आधुनिक विज्ञान और समाज अध्ययन के भाषा की एक बड़ी समस्या है कि इसमें ‘मन’ की कोई समझ नहीं है। जब कोई ‘मन की बात’ करता है तो इसका क्या मतलब होता है? जब कोई कहता है कि मेरे मन में एक बात आ रही है या कहता है कि मेरा मन ख़राब हो रहा है या फिर किसी व्यक्ति के बारे में कहता है कि मेरे मन से उतर गया या मेरा मन वहाँ खूब लगता है, तो इन सब में ‘मन’ का क्या मतलब है? मन की सुनो, मन में जो आए वही करो आदि-आदि हमें अक्सर सुनने को मिलता है। और प्रवासी भारतीयों से ज़्यादा मन के बारे में बातें कौन करता है। निश्चित रूप से ‘मन’ हमारे अंदर की एक अनुभूति है, जिसका कोई रूप या आकार नहीं होता है। यह एक सूक्ष्म चीज़ है जिसके अस्तित्व को हम अनुभव तो कर सकते हैं लेकिन इसे देख और छू नहीं सकते हैं। मन की भी अपनी आँखे हैं, उनके कान हैं। एक तरह से समझें तो आदमी के अंदर का वह एक और आदमी है, जिसे बंगाल के बाऊल लोग कहते हैं ‘मोनेर मानुष’। इस लेख में प्रवासी भारतीय लोगों के इसी मन को समझने की कोशिश करना चाहता हूँ। किसी के मन को समझना तो कठिन है, लेकिन उसके अंदर झांकना असम्भव नही। ख़ास कर उनके मन में भारतीय संस्कृति, ज्ञान
परम्परा और राजनीति को लेकर जो ऊहापोह चल रहा है उसे समझना ज़्यादा कठिन नहीं है। प्रसिद्ध फ़्रांसीसी मनोवैज्ञानिक लकाँ ने इंसानी रिश्तों को समझने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट का उपयोग किया है जिससे प्रवासी मन को समझने में हमारी कुछ सहायता हो सकती है। लकाँ बताते हैं कि बच्चे प्रारम्भिक दौर में अपने शरीर को अपनी माँ के शरीर से अलग नहीं समझते हैं। अलग समझने की प्रक्रिया शुरू होती है – लगभग दस से अठारह महीने के बीच। इसलिए आप देखेंगे कि जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो एक ऐसी स्थिति आती है जब दर्पण में अपने आप को देख कर वह चकित होता है कि यह है कौन? कभी अपने आप को छूता है कभी दर्पण को और कभी अपनी माँ को। दरअसल वह पहली बार अपने अस्तित्व को अपनी माँ के अस्तित्व से अलग समझने की प्रक्रिया से गुजर रहा होता है। लकाँ इसे मनुष्य के विकास का ‘मिरर स्टेज’ कहते हैं। यह बदलाव बच्चे के लिए सुखद नहीं होता। इसके बाद बच्चा अपनी माँ से और ज़्यादा लगाव महसूस करता है। इस लगाव को लकाँ ‘इमागो’ कहता है। यह दूरी जितनी बढ़ती है मन में मोह उतना ज़्यादा पनपता है। मेरा मानना है कि यही बात संस्कृतियों के बारे में भी लागू होती है।
संस्कृतियाँ मनुष्य की माँ जैसी होती है। हम जब तक उसमें घुले-मिले रहते हैं उसकी समझ अलग से नहीं बनती है। जब उसका अभाव होने लगता है तो हमें उसकी यादें या समझ ज़्यादा होने लगती है। प्रवासी भारतीयों के साथ ऐसा ही कुछ होता है। अपने वतन को छोड़ने की लाचारी भी होती है और वतन के छूट जाने का ग़म भी। वतन छोड़ना कोई आसान काम नहीं है। परिवेश की अर्थव्यवस्था, अच्छे रोजगार की तलाश या अभाव और सामाजिक असमानता जैसे कई कारणों से लोग गाँव या शहर छोड़ बाहर जाते हैं। वहां पहुंचकर उन्हें सब कुछ तो मिल जाता है, लेकिन वह संस्कृति व परिवेश जिसमें वह जन्म लेते हैं, जो रक्त के साथ घुल कर उनकी धमनियों में बहती हैं, उसका अभाव खटकता रहता है। उनके मन की दुविधा यह है कि वहां जा भी नहीं सकते हैं और उसके बिना रह भी नहीं सकते हैं। मन देश और विदेश के बीच पेंडुलम की तरह डोलता रहता है। सपने में गांव नज़र आता है और जागने पर शहर में अपना भविष्य। प्रवासी भारतीयों का मन इसी द्वंद में आजीवन उलझा रहता है। इसी द्वंद या दुविधा का इस्तेमाल सामाजिक संगठनों को बनाने में होता है और कई बार राजनैतिक संगठनों के समर्थन में भी। संस्कृति के प्रति जो प्रेम है
उसके दुरुपयोग की भी उतनी ही संभावना है। स्वदेश प्रेम में लोग धृतराष्ट्र बन जाते हैं और न्याय अन्याय के बीच का फर्क भी भूल जाते हैं और अंध राष्ट्रवाद का भी शिकार हो जाते हैं।
इसलिए जब देश में राष्ट्रवाद धीरे-धीरे अस्मिता की राजनीति में बदलने लगता है ‘इमागो’ के कारण प्रवासी लोग उसे देख नहीं पाते हैं। जब तक यह समझ आता है समय गुजर गया होता है। अन्य समाज में अर्थोपार्जन तो किया जा सकता है लेकिन लोगों की हालत वैसी ही हो जाती है जैसे मीठे पानी के तालाब की मछली को निकाल कर विशाल समुद्र के खारे पानी में डाल दिया गया हो। एक बार कोपेनहेगेन के रेलवे स्टेशन पर मैं ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था। मेरे अलावा केवल एक और यात्री था जो अफ़्रीका के किसी देश का निवासी था। ट्रेन आने में देर थी। मैं एक आम हिंदुस्तानी की तरह उसके क़रीब गया और उससे बातचीत करने लगा। मैने पूछा कि यह शहर उन्हें कैसा लगा। उनके जवाब कि ‘पिछले दस वर्षों में मैं पहला आदमी था जिसे उनके बारे में जानने
में कोई दिलचस्पी दिखी’ ने मुझे चकित कर दिया। काफ़ी समय तक वह अपने गांव के परिवेश और अपनों से बिछुड़ जाने की कहानियाँ सुनाता रहा। मै उसकी दिलचस्प कहानियाँ सुनता रहा और प्रवासी भारतीयों के मानस की तुलना उनसे करता रहा। अलगाव का यह दर्द उनके अंदर भी है और अपने लोगों के साथ जुड़े रहने का मन उनका भी है। लेकिन उसमें एक और दुविधा है। कई बार उन्हें लगता है कि जिन लोगों को, जिस समय को और जिस परिवेश व समाज को वे पीछे छोड़ आये हैं, उसमें वापस जाना सम्भव नहीं है। बीच-बीच में वापस जाने का उनका अनुभव भी ठीक नहीं रहा है। इससे उनका अलगाव और बढ़ ही जाता
है।
प्रवासी भारतीयों को राष्ट्र सेवा करने का मन हो ये लाज़िमी है। उनके मन में जो अलगाव का दर्द है, एक तरह से राष्ट्र सेवा उसकी दवा है। लेकिन इस दवा का सेवन सही तरीक़े से हो बहुत ज़रूरी है। इसमें पहली सावधानी यह रखने की जरूरत है कि हम अपने राष्ट्रवाद की समझ को सहेज कर रखें। राष्ट्रवाद संस्कृति प्रेम तो है लेकिन यह प्रेम किसी सांस्कृतिक अस्मितावाद और फिर धार्मिक उन्माद या सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में न परिणत हो जाए। उन्हें अपने देश में चल रही राजनीति की सही समझ होनी चाहिए और साथ ही देश के आर्थिक सामाजिक संरचनाओं की भी। इसके लिए उन्हें सरल भाषा में भारतीय राजनीति और अन्य विषयों पर लिखी सारगर्भित पुस्तकों की सहायता भी ली जानी चाहिए। बौद्धिक विमर्श को सांस्कृतिक गोष्ठियों का हिस्सा बनाना चाहिए। दूसरा तरीक़ा हो सकता है अपने समाज के लिए कुछ सामूहिक काम करना। हो सके तो अपनी आमदनी का एक हिस्सा भारत के उन लोगों पर खर्च करें जिन्हें वाकई इसकी जरूरत है। भारत के युवा छात्रों के संगठनों से जुड़ कर उन्हें बड़ा सोचने में मदद करना भी एक बेहतर तरीक़ा हो सकता है, राष्ट्र के प्रति अपने सम्मान को व्यक्त करने का। अपने समाज की अगली पीढ़ी से जुड़े रहने का यह सबसे अच्छा तरीक़ा हो सकता है। और तीसरा तरीक़ा हो सकता है प्रवासी भारतीयों के अनुभवों को साझा करना। यह प्रवासियों के जीवन संघर्ष को अगली पीढ़ी के लिए संजोये रखने की प्रक्रिया हो सकती है।
लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तरीक़ा हो सकता है भारतीय ज्ञान परम्परा से अपने संबंध को बनाए रखना। सम्भव है कि जो लोग विदेश जाते हैं उन्हें भारतीय ज्ञान परम्परा के बारे में पर्याप्त जानकारी न हो। यदि प्रवासी भारतीय इन ज्ञान परम्पराओं के बारे में जानकारी हासिल करें, दूसरों से साझा करें और इसके प्रचार प्रसार में सहयोग दें तो यह भारत की ही नहीं बल्कि मानवता की सेवा होगी। पश्चिमी समाज जिस दार्शनिक संकट से गुजर रहा है उसका निदान भारतीय ज्ञान परम्परा में खोजने का दायित्व
भारतीय प्रवासियों का है। संस्कृति प्रेम का उद्गार अक्सर केवल कर्म कांड में होते देखा गया है पर सच्चा और वास्तविक संस्कृति प्रेम को ज्ञान कांड में संलग्न होना चाहिए। संस्कृति मनुष्य की माँ है और ज्ञान सम्पदा किसी भी संस्कृति की आत्मा होती है। यदि प्रवासी भारतीय देश की उस आत्मा से प्रेम करें उसके सच्चे स्वरूप को समझें और उसकी पवित्रता से अपने नए समाज को अवगत करायें तो यही सही राष्ट्र्भक्ति होगी। इस से भारत का भौगोलिक विस्तार नहीं बल्कि सांस्कृतिक विस्तार होगा। यही भारत के राष्ट्रप्रेम की परम्परा रही है। सम्राट अशोक ने अपने समय में बुद्ध के ज्ञान को दुनिया भर में बाँटा था। आज दुनिया को पुनः भारतीय ज्ञान सम्पदा की ज़रूरत है और भारत के लोगों ने बहुत संघर्ष कर उसे मानव कल्याण के लिए सुरक्षित रखा है।